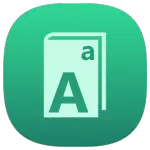अव्यय किसे कहते कहते हैं?
अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है –‘अ’+ ‘व्यय’ अर्थात जिसका कभी व्यय न हो।
जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई विकार पैदा नहीं है उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं
अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है- जो व्यय नहीं होता है अर्थात् ये अविकारी होते हैं ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होते हैं वहाँ एक ही रूप में रहते हैं जैसे- अन्दर बाहर अनुसारअधीन इसलिए यद्यपि तथापि, परन्तु आदि
जैसे – किन्तु , परन्तु ,यथा ,तथा ,लेकिन, अगर, मगर, इसलिए ,अतः, अतएव, वाह,आह , कब, क्यों ,इधर, उधर ,यहाँ,वहाँ इत्यादि।
अव्यय के भेद | Avyay ke bhed
अव्यय के चार प्रकार होते है –
1. क्रिया विशेषण अव्यय शब्द
2. सम्बन्धबोधक अव्ययय शब्द
3. समुच्चयबोधक अव्यय शब्द
4. विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द
अन्य भेदों में निपात व अव्ययीभाव समास के उदाहरण है।
1. क्रिया विशेषण अव्यय शब्द
क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं जैसे- ‘अधिक तेज दौड़ना में दौड़ने की विशेषता क्रिया विशेषण शब्द तेज’ बतला रहा है परन्तु ‘अधिक’ क्रिया विशेषण शब्द की विशेषता बतला रहा है अन्य उदाहरण
- वह प्रतिदिन पढ़ता है।
- कुछ खा लो।
- मोहन सुन्दर लिखता है।
- घोड़ा तेज दौड़ता है
- कछुआ धीरे-धीरे चलता है।
- घोडा तेज दौड़ता है।
इन वाक्यों में प्रतिदिन कुछ सुन्दर व तेज शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं अतः ये शब्द क्रिया-विशेषण अव्यय हैं
उपर्युक्त वाक्यों में ‘धीरे-धीरे’ और ‘तेज’ शब्द चलना व दौड़ना क्रियाओं की विशेषता बता रहे है ,अतः ये क्रिया विशेषण शब्द माने जाते है।
क्रिया-विशेषण अव्यय छः प्रकार के होते हैं-
(1 ) स्थानवाचक क्रिया विशेषण-
जिस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया की स्थान या दिशा सम्बन्धी विशेषता प्रकट होती हैवह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है जैसे-
- वह यहाँ नहीं है
- तुम वहाँ क्या कर रहे थे?
- तुम आगे चलो
- वह पेड़ के नीचे बैठा है
- इधर-उधर मत भागो।
- हमारे आस-पास रहना।
इन वाक्यों में यहाँवहाँ, नीचे, इधर-उधर, आस-पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं
(2 ) काल वाचक क्रिया-विशेषण अव्यय-
जिन क्रिया-विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय या काल मालूम होता हैउन्हें कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे- सर्वदा, बहुधा, निरन्तर प्रतिदिन,आज कल परसों आदि
- तुम अब जा सकते हो
- दिन भर पानी बरसता रहा।
- तुम प्रतिदिन समय पर आते हो।
इन वाक्यों में अब, दिनभर, प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं।
(3) परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय-
जिन क्रिया-विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अर्थात् अधिकता-न्यूनता, नाप-तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे- थोड़ा तनिक, पर्याप्त, बहुत, बिल्कुल आदि।
- उतना खाओ, जितना आवश्यक हो।
- कुछ तेज चलो।
- तुम खूब खेलो।
- रमेश बहुत बोलता है
इन वाक्यों में उतना, जितना, कुछ, खूब व बहुत परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय हैं।
(4) रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय-
वे क्रिया-विशेषण शब्द जिनसे क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है अर्थात् क्रिया के होने का ढंग मालूम होता है उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय कहते हैं जैसे—धीरे-धीरे मानो, यथा शक्ति , ज्यों, त्यों आदि
रीतिवाचक विशेषण निम्न अर्थों में आते हैं-
1.प्रकारात्मक धीरे-धीरे अचानक, अनाया ससंयोग से एका एक सहसा, सुख पूर्वक, शान्ति से हँसता हुआ, मन से धड़ाधड़, झटपट, आप ही आप शीघ्रता से ध्यानपूर्वक, जल्दी, तुरन्त आदि।
2. निश्चयात्मक अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, वास्तव मेंबेशकनिःसंदेह आदि।
3. अनिश्चयात्मक-कदाचित्, शायदसम्भव हैबहुत करके, बहुधाप्रायः, अक्सर आदि।
4. स्वीकारात्मक- हाँठीकसचबिल्कुल सहीजी हाँ आदि।
5. कारणात्मक (हेतु)- इसलिए, अतएवक्यों, किसलिएकाहे कोअतः आदि।
6. निषेधात्मक-न, नानहींमतबिल्कुल नहीं, हरगिज नहींजी नहीं आदि।
7. आवृत्यात्मक-गटागट, फटाफट, खुल्लमखुल्ला आदि।
8. अवधारक-हीतोभीतक, भरमात्रअभी, कभी, जब भीतभी आदि।
(5) स्वीकारात्मक क्रिया-विशेषण अव्यय-
जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्वीकृति का बोध होता हैउन्हें स्वीकारात्मक क्रिया-विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे- जी, अवश्य, अच्छा, बहुत अच्छा, जरूर आदि
( 6) निषेधात्मक क्रिया-विशेषण अव्यय-
जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के निषेध का ज्ञान होता हैउन्हें निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैंजैसे-न, नहीं, मत आदि
क्रिया-विशेषणों की रचना :
मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्ययसमास आदि के योग से भी कुछ क्रिया-विशेषण शब्दों की रचना होती है जिन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये निम्न प्रकार हैं-
- संज्ञा से प्रेमपूर्वककुशलतापूर्वक, दिन-भर, रात-तक, सवेरेसायं आदि।
2. सर्वनाम से—यहाँवहाँ, अबजबजिससेइसलिएजिस परज्यों, त्यों, जैसे-वैसेजहाँ-वहाँ आदि।
3. विशेषण से -धीरेचुपके, इतने में ऐसे वैसे कैसे जैसे पहले, दूसरे, प्रायः बहुधा आदि।
4 . क्रिया से-चलते-चलते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, जाते-जाते करते हुए लौटते हुए आदि।
5. शब्दों की पुनरुक्ति से हाथों-हाथ, रातों-रातबीचों-बीच, घर-घर, साफ-साफ, कभी-कभीक्षण-क्षणपल-पल, धड़ाधड़ आदि।
6. विलोम शब्दों के योग से रात-दिन, साँझ-सवेरेदेश-विदेश, उल्टा-सीधाछोटा-बड़ा आदि।
7. तः प्रत्याना-सामान्यतः, वस्तुतः, साधारणतःयेन केन प्रकारेण (जैसे-तैसे) आदि।
8. बिना प्रत्ययान्त के-कभी-कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बिना किसी प्रत्यय केक्रिया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैंजैसे-
(1) संज्ञा –
- तू सिर पढ़ेगा।
- तुम खाक करोगे।
(2) सर्वनाम –
- यह क्या हुआ?
- तूने यह क्या किया?
(3) विशेषण –
- अच्छा हुआ
- घोड़ा अच्छा चलता है
(4) पूर्वकालिक क्रिया –
- सुनकर चला गया
- देखकर चकरा गया।
इस प्रकार के वाक्य क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं
कहाँ से आ रहे हो
( 9 ) परसर्ग जोड़कर कुछ क्रिया विशेषणों के साथ कीके, कोसेपर आदि विभक्तियाँ भी लगती हैं और इनके योग से भी क्रिया विशेषणों की रचना होती हैजैसे-
- यहाँ से क्यों जा रहे हो
- कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ।
- गुरुजी से नम्रता से बोलो
- आगे से ऐसा मत करना।
- रात को देर तक मत पढ़ना
परसगाँ की सहायता से बने ये वाक्य क्रिया-विशेषणों का कार्य कर रहे हैं
(10) पदबन्ध-पूरे वाक्यांश क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैंजैसे-
सवेरे से शाम तक।
तन-मन-धन से
जी-जान से
पहाड़ की तलहटी में।
आपके आदेशानुसारआदि पदबन्ध क्रिया विशेषण हैं
2. समुच्चयबोधक अव्यय-
जिन अव्यय शब्दों से दो शब्ददो वाक्यांश, दो उपवाक्यपदबन्ध या वाक्य जोड़े जाते हैंउन्हें समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं जैसे- पुनःयथा, वरना, अधिक आदि।
- वह निकम्मा है इसीलिए सब उसे दुत्कारते हैं
- यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होग
- राम यहाँ रहे या कहीं और।
- यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का।
उक्त वाक्यों में ‘इसीलिए’, ‘यदि’, ‘तो’, ‘या’, ‘और’ शब्द समुच्चय या योजक अव्यय हैं क्योंकि ये वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं।
समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं-
1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक
2. व्याधिकरण समुच्चय बोधक।
1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक-
वे अव्यय जो समान घटकों (शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों) को परस्पर मिलाते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं।
समानाधिकरण अव्यय के तीन भेद हैं-
(1) संयोजक-
जो शब्द वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों में संयोग प्रकट करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे-
- राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं।
- मैं और मेरा पुत्र एवं पड़ौसी सभी साथ थे।
- बादल उमड़े एवं वर्षा हुई।
उपर्युक्त वाक्यों में ‘और’, ‘एवं’ शब्द संयोजक अव्यय हैं।
(2) विकल्पबोधक-
ये अव्यय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए अथवा विभाजन करते हुए उनमें मेल कराते हैं। जैसे-
तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा।
न रमेश कोई काम करता है न सुरेश ही।
तुम्हें जन्मदिन पर घड़ी मिलेगी या साइकिल।
उक्त वाक्यों में ‘अथवा’, ‘न’ व ‘या’ शब्द विकल्पबोधक अव्यय का कार्य कर रहे हैं।
(3) भेदबोधक-
जो योजक शब्द एक वाक्य, वाक्यांश या शब्द से भिन्नता का ज्ञान कराते हैं उन्हे भेदबोधक कहते हैं। जैसे- परन्तु, यद्यपि, तथापि, चाहे, तो भी। • वह नालायक है फिर भी पास हो जाता है।
- यद्यपि तुम बुद्धिमान हो तथापि कम अंक लाते हो।
- तुम पढ़ने में होशियार हो परन्तु रोज नहीं आते।
उक्त वाक्यों में ‘फिर भी’, ‘यद्यपि’, ‘तथापि’ और ‘परन्तु’ शब्द वाक्यों में भिन्नता का ज्ञान करा रहे हैं।
भेदबोधक के भी चार निम्नलिखित उपभेद हैं-
(1) विरोधदर्शक-
जब संयोजक द्वारा पहले वाक्य से मनचाहे अर्थ का विरोध प्रकट हो, तब वह विरोधदर्शक कहलाता है। जैसे- किन्तु, परन्तु आदि। इनके पहले अल्पविराम (,) अर्द्धविराम (;) लगते हैं।
- रमेश ने बहुत प्रयत्न किया; परन्तु फिर भी असफल रहा।
- छात्राएँ आगे बढ़ती गई; किन्तु छात्र पिछड़ते रहे।
उक्त वाक्यों में मनचाहा अर्थ नहीं मिल पाया क्योंकि प्रयत्न करना सफलता का प्रतीक है; पर असफलता मिली। छात्राओं की तरह छात्र भी आगे बढ़ते पर ऐसा अर्थ नहीं मिला। इसलिए यहाँ विरोधदर्शक अव्यय ही क्रियाशील रहे।
(2) परिणामदर्शक-
इसके द्वारा मिला हुआ वाक्य किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। जैसे-
- चुप हो जाओ नहीं तो दण्ड मिलेगा।
- नौकर ने चोरी की थी इसलिए उसे निकाल दिया।
- मेरा कहना मानो अन्यथा बाद में पछताओगे।
उक्त वाक्यों में ‘नहीं तो’, ‘इसलिए’, ‘अन्यथा’ शब्द परिणाम दर्शक का कार्य कर रहे हैं।
( 3 ) संकेतबोधक
जहाँ दो वाक्यों के आरम्भ में संयोजक द्वारा अगले सम्बन्ध बोधक (योजक) का संकेत पाया जाए, वहाँ संकेत बोधक होता है। वाक्य में अव्यय प्रायः जोड़े में ही प्रयुक्त किए) जाते हैं। जैसे- •
- यद्यपि वह बहुत पढ़ा लिखा है तथापि रिश्वती होने के कारण उसका सम्मान नहीं है।
- यदि तुम गाँव जाओ तो वहाँ सबसे मेरा राम-राम कहना।
- चाहे कोई कितना धनी हो, तो भी चरित्र के बिना सम्मान नहीं पाता।
उक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि यद्यपि के साथ तथापि, यदि के साथ तो, चाहे के साथ तो भी, जब के साथ जब तक, से के साथ तक, भले के साथ परन्तु आदि का वाक्यों में प्रयोग होता है तो उक्त संकेतबोधक अव्यय कहलाएंगे।
(4) स्वरूपबोधक-
जिस शब्द का प्रयोग पहले आए शब्द, वाक्यांश या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाए, तो वह समुच्चय बोधक का स्वरूप बोधक नामक अव्यय भेद कहलाता है। जैसे-
- तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात् कोमल हैं।
- वह अहिंसावादी यानी गाँधीजी का पुजारी है।
- राम इतना अच्छा है मानो सचमुच राम है।
इन वाक्यों में यानी, अर्थात्, मानो स्वरूप बोधक अव्यय हैं।
2. व्याधिकरण समुच्चय बोधक-
एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे- यदितोयद्यपितथापिताकि, इसलिए, यानिअर्थात् आदि
व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय चार प्रकार के होते हैं-
(i) कारणबोधक-
(क्योंकि, चूंकिइसलिए, किताकि आदि)
ये अव्यय वाक्यों के आरंभ में आते हैं। जैसे-
- अजय को बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा
- मुझे घर जाना चाहिए ताकि मैं आराम कर सकूँ।
(ii) संकेत बोधक-
(यदि, तो, यद्यपि… तथापियद्यपि… परंतु आदि)
ये अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं जैसे-
- यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी कम नहीं हुई।
- यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ।
(III) स्वरूप बोधक-
(अर्थातयानिमानो आदि)
ये अव्यय पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। जैसे-
- तुम्हारे हाथ फूल जैसे अर्थात् कोमल हैं।
- मैं अहिंसावादी यानि गाँधी का समर्थक हूँ।
(IV) उद्देश्य बोधक-
(ताकि, जिससेकिइसलिए आदि।)
ये अव्यय आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य वाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैंजैसे-
- मैंने सुबह पढ़ाई पूरी कर ली ताकि शाम को खेल सकूँ
- मैं भागा जिससे गाड़ी पकड़ सकूँ।
3. सम्बन्ध बोधक अव्यय-
जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं एवं उनका सम्बन्ध वाक्य के दूसरे शब्दों या पदों के साथ बताते हैं, उन्हें सम्बन्ध बोधक अव्यय कहते हैं जैसे- ओर अपेक्षा, तुल्य, वास्ते, विशेष पलटे ऐसा, जैसे लिए मारे, करके आदि सम्बन्धवाचक अव्यय हैं उदाहरण-
खुशी के मारे वह पागल हो गया।
बालक चाँद की ओर देख रहा था
मेरे घर के सामने मन्दिर है
छत के ऊपर मोर नाच रहा है
मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई
उक्त वाक्यों में मारेओरसामनेऊपर, कारण शब्द सम्बन्ध बोधक अव्यय का कार्य कर रहे हैंइनके अतिरिक्त निम्नलिखित सम्बन्ध बोधक शब्द और उनके प्रयोग द्रष्टव्य हैं-
शब्द – प्रयोग
- नाईं पढ़े-लिखे की नाई (तरह)
- रहे दो घडी दिन रहे चल देना
- नीचे पेड़ के नीचे खाट पर सो जाना
- तले- गरीब आकाश तले रात गुजारते हैं।
- पास-गाँव के पास स्टेशन है
- निकट-शहर के निकट के लोग प्रायः सम्पन्न होते हैं
- निमित्त-हम सब तो निमित्त मात्र हैं
- आगे- मेरे घर के आगे बस स्टेण्ड है
- पीछे- हमारे घर के पीछे बगीचा है
- पहले वर्षा से पहले छत ठीक कर लो।
- द्वारा मेरे द्वारा कुछ गलत न हो जाए।
- समान-ज्ञान के समान और कोई पवित्र वस्तु नहीं है
- समीप-तालाब के समीप मत जाना।
- तक हम दो दिन तक भटकते रहे
- प्रतिकूल-प्रकृति प्रतिकूल चले तो विनाश हो जाएगा
- विरुद्ध मेरे विरुद्ध वह आवाज नहीं उठा सकता।
- मध्य-आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य मन मुटाव चल रहा है
- विषय-मुझे उसके विषय में कुछ नहीं मालूम
- बाहर-घर के बाहर बहुत बड़ा चौक है
- परे-शक्ति से परे व्यक्ति को कुछ नहीं करना चाहिए
- समेत भाइयों के समेत मैं भी वहीं था
- तुल्य-वह मानव नहीं देवता-तुल्य है
- सदृश-वह खुशी के मारे कमल के सदृश खिल उठा
सम्बन्ध बोधक अव्यय के भेद-
सम्बन्धबोधक अव्ययों के भण्डार को भाषा की सुविधा हेतु चौदह भेदों में इस प्रकार स्पष्ट करेंगे-
1 . कालवाचक – आगेपीछेपहले, बादपूर्वपश्चात्, उपरान्त आदि
2. स्थानवाचक – पास, दूरतरफप्रतिऊपर, नीचे, तले, मध्य, बाहर हीभीतर, अन्दर, सामने, निकट, यहाँवहाँ, नजदीक आदि।
3. साधनवाचक – हाथ, द्वाराहस्ते, विरुद्ध, जरियेमारफतसहारे आदि।
4. दिशावाचक – सामनेओरपारतरफआर-पारप्रति, आस-पास आदि
5. विरोधसूचक – प्रतिकूल, उलटेविपरीत, खिलाफ आदि
6. हेतु (कारण) वाचक कारणहेतुलिए, निमित्तवास्तेखातिर आदि।
7. व्यतिरेकवाचक – अतिरिक्त, अलावासहितसिवाय आदि
8. सहसूचक साथ, संगसमेत, पूर्वक, अधीनवश आदि।
9. पार्थक्य सूचक – दूरपृथक्त, परेहटकर आदि
10. तुलनावाचक – की अपेक्षाकी बजायवनिस्पत आदि।
11. संग्रहवाचक – मात्रभरपर्याप्त, तक आदि
12. साम्यवाचक – सदृशबराबरऐसाजैसाअनुसारसमान, तुल्य, नाई, अनुरूपतरह आदि
13. विनिमयवाचक – एवजपलटेके बदलेकी जगह आदि
14विषयकवाचक भरोसे, लेखे, नाम, विषयबाबत आदि।
4. विस्मयादिबोधक अव्यय-
वे अव्यय शब्द जो बोलने वाले या लिखने वाले के विस्मय हर्ष शोक लज्जा ग्लानि खेद आदि मनोभावों को प्रकट करते हैंविस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं जैसे- अहो हे,छी,वाह,धिक्कार आदि
विस्मय बोधक अव्यय के सात भेद हैं-
- हर्षबोधक वाह-वाह!, धन्य-धन्य!, आहा!शाबाश!
2. शोकबोधक-हाय!आह!, हा हा!त्राहि-त्राहि!
3.आश्चर्यबोधक-अहोओहओहो!हैक्या!
4. अनुमोदनबोधक- अच्छा!, हाँ हाँ!वाह!शाबाश!
5.तिरस्कारबोधक-छिःहट!अरेधिक!
6.स्वीकृतिबोधक-अच्छा!ठीक!, बहुत अच्छा!हाँ!जी हाँ!
7.सम्बन्धबोधक अरेरे!अजी! अहोआदि।
कभी-कभी संज्ञा, सर्वनामविशेषण आदि शब्द भी विस्मयादिबोधक का काम करते हैं जैसे-
- संज्ञा-राम-रामा, शिव-शिव!जय गंगे!, श्री कृष्णआदि।
- सर्वनाम-यही!, कौन!क्या!तूने! आदि।
- विशेषण-सुन्दर!अच्छा!, खूब!, बहुत अच्छे !, जंगली! आदि।
- क्रिया-चला जाऊँ!चुपआ गये! आदि।
- वाक्यांश-शान्तम् पापम्! आदि।
निपात-
वे सहायक पद जो वाक्यार्थ में नवीन अर्थ या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैंनिपात कहलाते हैं। जैसे ही तक, तोभी, सा, जी, मत, यह, क्या आदि निपात हैं।
निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं हैं। इनका कोई भी लिंग या वचन नहीं होतानिपात का कार्य शब्द-समूह को बल प्रदान करना है।
निपात के भेद-
- स्वीकारात्मक-हाँजी, जी हाँ
- नकारात्मक-जी नहीं, नहीं।
- निषेधात्मक मत।
- प्रश्नबोधक क्या।
- विस्मयात्मक-काश।
- तुलनात्मक-सा।
- अवधारणात्मक-ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन।
- आदरात्मक-जी।